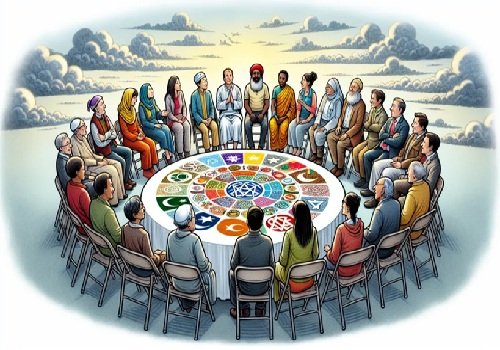गौतम चौधरी
तेज़ी से बदल रही दुनिया में धार्मिक विविधता, हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। हम देखते हैं कि लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, यहूदी आदि, जिनकी अपनी-अपनी मान्यताएँ, परंपराएँ और आचार व व्यवहार होते हैं। हालांकि ये धर्म ऊपर से अलग दिखते हैं, लेकिन ये अक्सर शांति, प्रेम, दया और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे साझा मूल्यों के आधारभूत संरचना पर ही आरूढ़ होते हैं। फिर भी, गलतफहमियों, जानकारी की कमी, विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह और कभी-कभी राजनीति के कारण धर्म संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे में अंतर-धार्मिक संवाद का महत्व बढ़ जाता है। यह हमें एक-दूसरे को समझने और शांति से साथ रहने में मदद करता है।
अंतर-धार्मिक संवाद का अर्थ है – अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच खुला और सम्मानजनक संवाद। यह किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की बहस नहीं है, बल्कि यह सुनने, समझने और सीखने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य, आपसी सम्मान बढ़ाना, नफरत कम करना, और ऐसा समाज बनाना जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यहां यह भी समझना चाहिए कि जब परमात्मा एक है तो उसने जिस किसी को बनाया वह सब उसी की संरचना है। उन संरचनाओं में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो परमपिता को ही हानि पहुंचती है। इसलिए आपसी संवाद से ही यह तय होगा कि आधिर ईश्वर और उसके द्वारा रचा गया संचार कितना व्यापक और संवेदनशील है।
धार्मिक मतभेदों के कारण अक्सर अविश्वास, घृणा और हिंसा देखी गई है। हम अकसर सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक तनावों और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के बारे में सुनते हैं, जो प्रायः अन्य धर्मों के प्रति गलतफहमियों पर आधारित होते हैं। जब व्यक्ति अन्य धर्मों के बारे में नहीं जानते, तो झूठी बातों पर विश्वास करना या नफ़रत से प्रभावित होना आसान हो जाता है। अंतर-धार्मिक संवाद गलत धारणाओं की दीवारों को तोड़ता है, समुदायों के बीच मित्रता बनाता है, एक-दूसरे के विश्वास और मूल्यों को समझने में मदद करता है और शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे सामान्य लक्ष्यों पर साथ मिलकर काम करने का रास्ता खोलता है। इससे शांति और एकता को बढ़ावा मिलता है और अज्ञान या डर से होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।
अंतर-धार्मिक संवाद का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे यह पता चलता है कि सभी धर्मों की शिक्षाओं में कई समानताएँ हैं। अधिकतर धर्म शांति और अहिंसा, करुणा और दान, सत्य और ईमानदारी, बुजुर्गों का सम्मान, गरीबों की सेवा, क्षमा और विनम्रता की बात करते हैं। जैसे – हिंदू धर्म ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की बात करता है (सारा संसार एक परिवार है), इस्लाम रहमा (दया) और सलाम (शांति) पर ज़ोर देता है, ईसाई धर्म अपने पड़ोसी से प्रेम करो सिखाता है, बौद्ध धर्म अहिंसा और सचेतनता का समर्थन करता है, सिख धर्म सर्वत दा भला (सबकी भलाई) की बात करता है और जैन धर्म अपरिग्रह (त्याग) और शांतिपूर्ण जीवन पर बल देता है। जब लोग धर्म की सीमाओं से परे बात करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे उतने अलग नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था, या बताया जाता है। यह एक साझा मानवता की भावना को जन्म देता है, जो साम्प्रदायिक सौहार्द की नींव है।
हम विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को कई तरीकों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी सम्मानपूर्वक और तथ्यात्मक रूप से दी जानी चाहिए। जब युवा सभी विश्वासों की सुंदरता को समझते हुए बड़े होते हैं, तो वे दूसरों से नफ़रत नहीं करते। विभिन्न धर्मों के लोगों को साथ लाकर त्योहारों, संगोष्ठियों या कार्यशालाओं का आयोजन समझ को बढ़ाता है। एक-दूसरे के त्योहार मिलकर मनाना खुशी और दोस्ती को बढ़ाता है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि के धर्मगुरुओं का समाज पर बड़ा प्रभाव होता है। जब वे एकजुटता की बात करते हैं, तो लोग सुनते हैं। वे अपने अनुयायियों को सहिष्णुता और शांति की राह दिखा सकते हैं। मीडिया नफ़रत फैलाने के बजाय एकता और सहयोग की कहानियाँ दिखा सकती है। फिल्में, लेख और सोशल मीडिया एकता और साझा मूल्यों की शक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। युवा पीढ़ी समाज का भविष्य है। छात्रों और युवाओं के लिए विशेष संवाद सत्र या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बना सकते हैं। जब लोग मिलकर सेवा करते हैं, तो वे अपने मतभेद भूल जाते हैं। सेवा का मूल्य सभी धर्म साझा करते हैं।
वर्तमान भारत, भले साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, फिर भी धार्मिक सौहार्द की कई प्रेरक कहानियाँ प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई अक्सर एक-दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। पंजाब में मुसलमानों और सिखों ने मिलकर मस्जिदों और गुरुद्वारों की मरम्मत की है। ईद या दीवाली पर विभिन्न समुदायों के लोग मिठाइयाँ और शुभकामनाएँ बाँटते हैं। झारखंड के हजारीबाग में रामनौमी का झंडा मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे सांप्रदायिक सदभाव के उदाहरण भरे पड़े हैं। अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरु हिंसा रोकने के लिए एक साथ शांति यात्राएँ भी निकाल सकते हैं, जिसमें केवल सौहार्द और साम्प्रदायिक सदभाव पर ही चर्चा हो।
अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना हमेशा आसान नहीं होता। इस क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। समाज में अब भी बहुत सी अज्ञानता, पूर्वाग्रह और संदेह मौजूद हैं। राजनीतिक एजेंडा कभी-कभी धर्म का दुरुपयोग कर लोगों को बाँटता है। कुछ लोग डरते हैं कि अन्य धर्मों से संवाद करना उनके अपने विश्वास को कमजोर कर देगा। लेकिन संवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम हर बात से सहमत हों। यह असहमति के बावजूद एक-दूसरे का सम्मान करना है। सच्चा धर्म खुलापन, नम्रता और करुणा सिखाता है। एक मजबूत विश्वास सीखने से नहीं डरता। इसलिए खुद के विश्वास को कमजोर होने वाली थ्योरी निराधार है।
अंतर-धार्मिक संवाद केवल धर्म का विषय नहीं है – यह एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने की प्रक्रिया है, जहाँ हर व्यक्ति सम्मानित और सम्मिलित महसूस करे। यह डर और नफ़रत को मिटाने का एक सशक्त साधन है। जब विभिन्न धर्मों के लोग आपस में बात करते हैं, सुनते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं, तो वे सौहार्द के बीज बोते हैं। ये बीज एकता और शांति के मजबूत वृक्षों में बदलते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में और एक ऐसे विश्व में जो तेजी से जुड़ता जा रहा है, अंतर-धार्मिक संवाद कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इसलिए सांप्रदायिक सदभाव के लिए संवाद का सिलसिला प्रारंभ करना यथेष्ट रहेगा।