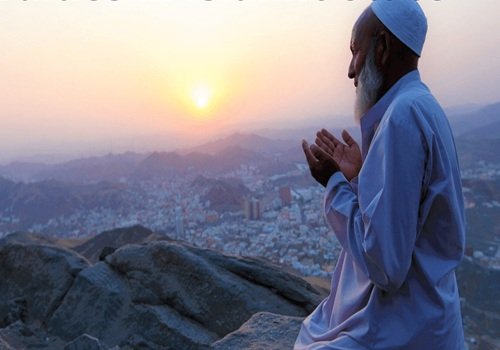गौतम चौधरी
इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतों का जब हम निचोर निकालते हैं तो हमें धार्मिक और सामाजिक चिंतन से ज्यादा यह एक राजनीतिक समावेशी समाज के निर्माण की संकल्पना जान पड़ता है। इस्लाम के अंतिम पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे व आलिहि व सल्लम मोहम्मद पैगंबर मक्का में, यहाँ तक कि काबा के परिसर में भी क़ुरआन के उपदेश देने लगे और उन्हें सुनने वालों की तादाद धीरे-धीरे बढ़ने लगी तो तत्कालीन अरब-समाज में हलचलें पैदा हुईं। अगर उनके संदेश का स्वरूप गुढ रहस्यवाद और आध्यात्मिक ही रहता तो पारंपरिक अरबी समाज और सत्ता में बैठे रसूख़दारों को इससे अधिक आपत्ति न होती, किन्तु उनके कानों पर तब जूँ रेंगीं जब मोहम्मद के उपदेश सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों में प्रवेश करने लगे।
मक्का के तत्कालीन बहुदेववादी और मूर्तिपूजक रसूख़दारों को मोहम्मद के एकेश्वरवाद के उपदेश ने जितना तंग किया, उससे ज़्यादा वो मोहम्मद के राजनैतिक बयानों से परेशान हो रहे थे। मोहम्मद ग़ैर-बराबरी और नाइंसाफ़ी की ज़ोरदार मुख़ालिफ़त कर रहे थे, मज़लूमों और ख़ासकर यतीमों की मदद करने का विचार उनके दिल के क़रीब था। उनके उपदेशों से यह जान पड़ता है कि वे धन-संग्रह की सरमायेदारी प्रवृत्तियों के विरोधी थे और ज़कात की समर्थक थे। तत्कालीन अरब-समाज के नामी-गिरामियों को मोहम्मद की इन बातों में बग़ावत की बू आने लगी। यही कारण है कि तत्कालिन अरबी पारंपरिक समाज ने मोहम्मद की मुखाल्फत प्रारंभ कर दी।
ज़रा क़ुरआन की इन आयतों पर ग़ौर फ़रमाइये –
‘‘जिन्होंने सच्चाई से पीठ फेरी और दौलत इकट्ठा करके उसको ताले में बंद कर दिया, उनको क़ुरआन बुलाकर कहती है…’’ (70: 17-18)
‘‘जो फ़कीरों और मज़लूमों को ज़कात देते हैं…’’ (70: 24-25)
‘‘और हम ये चाहते थे कि कमज़ोरों का साथ दें और उन्हीं को वारिस बनाएँ।’’ (28: 5)
‘‘जो दौलत जमा करते हैं और अपने पैसों की मुसलसल गिनती करते फिरते हैं, उन्हें क्या लगता है वो दुनिया-फ़ानी में हमेशा जीते रहेंगे?’’ (104: 2-3)
‘‘फ़ुज़ूलख़र्च मत करो। यक़ीनन, ख़ुदा बेजा ख़र्च करने वालों को पसंद नहीं करता।’’ (6: 141)
उक्त कुरानी आयतों के कारण ही वामपंथी मुस्लिमों ने इस्लामिक व्यवस्था को कल्याणकारी राज व्यवस्था का पहला संगठित स्वरूप बताया है। इन्हीं तमाम आयतों के हवाले से इस्लामिक-सोशलिज़्म के विचार की स्थापना की गयी और यह रेखांकित किया गया कि वेलफ़ेयर-स्टेट का विचार इस्लाम के मूल में है।
मोहम्मद का यह संदेश कि ख़ुदा के सामने सब बराबर हैं, ज़ात, नस्ल और दौलत की बुनियाद पर किसी में कोई ऊँच-नीच नहीं है, उस वक़्त के अरब-समाज के हाशिये के लोगों के दिलों को छू गया था। इससे इस्लाम की तत्कालीन अरब-समाज की परिस्थितियों में एक क्रांतिकारी भूमिका परिलक्षित होती है। इतिहासकार गिबन ने तो इस्लाम के उदय को ‘‘एक ऐसी अविस्मरणीय क्रांति’’ बताया, जिसने ‘‘दुनियाभर के मुल्कों के राष्ट्रीय-चरित्र पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।’’ महान साम्यवादी चिंतक मानवेन्द्र नाथ राय ने कहा है कि ‘‘इस्लाम का उदय धार्मिक दमन के विरुद्ध पीड़ित लोगों के संरक्षण के रूप में हुआ था।’’ इलहाम से पहले का ख़ुद मोहम्मद का जीवन-चरित्र इसकी मिसाल देता है कि कैसे वो कारोबार में ईमानदारी को सर्वाेच्च मूल्य मानते थे, चीज़ों को वाजिब दामों पर बेचने की हिमायत करते थे और मुनाफ़े का हिस्सा ज़रूरतमंदों को तक़सीम कर देने की बात करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा करके भी दिखाया, जबकि उन दिनों उनके पास दौलत नहीं थे।
मोहम्मद के इस विचार के कारण मक्का के ताक़तवर रसूख़दारों के द्वारा अबू-तालिब पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो मोहम्मद को हिदायत दें या हाशिम क़ुनबे से निकाल बाहर कर दें। क़ुनबे से निकाल बाहर कर देने का मतलब उस ज़माने में यह था कि अगर तब ज़ात-बदर शख़्स का क़त्ल कर दिया जाए तो उसकी मौत का इंतक़ाम लेना उसके क़ुनबे के लिए फ़र्ज़ नहीं होगा। जब अबू-तालिब ने मोहम्मद को समझाने के लिए बुलाया और उनसे अर्ज़ किया कि ऐसे खुलकर ये तमाम बातें ना बोलें, जिससे खुद के समाज में परेशानी हो। तब मोहम्मद ने जवाब दिया- ‘‘अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चाँद रख दिया जाए, तब भी मैं हक़ की राह से पीछे ना हटूँगा, फिर चाहे मेरा क़त्ल ही क्यों ना कर दिया जाए!’’
इतिहासकार अल-तबरी का बयान है कि ऐसा कहते हुए मोहम्मद की आँखें डबडबा गईं और वो दरवाज़े की ओर बढ़े। तब अबू-तालिब ने रूंधे गले से उन्हें रोका और कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोडूँगा। उन्होंने ताउम्र ये वादा निभाया भी, हालाँकि वो ख़ुद बुतपरस्त थे और उन्होंने ख़ुद कभी इस्लाम क़ुबूल नहीं किया।
मोहम्मद को डराने-धमकाने और लालच देकर ख़रीदने तक की कोशिशें की गईं, लेकिन सब नाकाम रहीं। इतिहास गवाह है कि उस दौर की तमाम ज़िल्लत का सामना मोहम्मद ने सब्र, ख़ामोशी और यहाँ तक कि पूरी अहिंसा के साथ किया। एक बार तो मोहम्मद दुआ में बैठे थे और अबू-जहल नाम का उनका एक विरोधी उनके सामने खड़े होकर उन्हें गालियाँ बक रहा था। इस तरह के दृश्यों ने आम लोगों के मन में मोहम्मद के प्रति हमदर्दी बढ़ा दी। जैसा कि लेज़्ली हैज़ल्टन ने मोहम्मद की बायोग्राफ़ी में लिखा है – ‘‘मोहम्मद का ज़ोर क़ुरआन के संदेश पर था, लेकिन उनके विरोधियों का ज़ोर मोहम्मद पर था। मोहम्मद ने बार-बार कहा था कि मैं सब लोगों से अलग नहीं हूँ, लेकिन उनके विरोधियों ने उनकी मुख़ालिफ़त कर-करके उन्हें आमजन की नज़र में विशिष्ट बना दिया।’’
यही वो दौर था, जब मोहम्मद के समर्थकों और इस्लाम क़बूल करने वालों में कुछ अहम नाम जुड़े और जिन्होंने मोहम्मद की तरफ़ शक्ति-संतुलन को झुका दिया। इनमें कुछ दूरदर्शी रणनीतिकार और दुर्द्धर्ष योद्धा भी थे, जो आगे चलकर इस्लाम की बुनियाद को मज़बूत बनाने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे रणनीतिकार सहाबा कहलाए। इसमें अहम नाम, हजरत अबू-बकर सिद्दकी, हज़रत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली का नाम सुमार है। इन सहाबाओं ने इस्लाम की बुनियाद को इतना मजबूत कर दिया कि वह आज तक दुनिया को प्रकाश और प्रभाव प्रेषित कर रहा है।