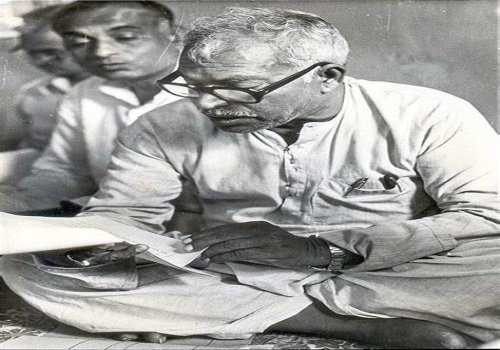विवेक
भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, आदि पुरस्कारों का वैसे तो आम मेहनतकश जनता के लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। चूँकि भारत रत्न और इस प्रकार के पुरस्कार प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति की अनुशंसा पर दिये जाते है, अतः सत्ता में रहने वाली पार्टी अक्सर अपने किसी पुराने नेता या उनकी राजनीति से सहमति रखने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न देकर अपनी साख मजबूत करने का प्रयास करती है। एक समय के बाद, इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों का जिक्र सामान्य ज्ञान की किताबों तक सीमित हो जाता है। लेकिन जितनी चतुराई से मोदी सरकार ने इन पुरस्कारों का इस्तेमाल किया है, वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ है।
राम मन्दिर उद्घाटन के तुरन्त बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करना भोले-भाले लोगों को आश्चर्यजनक फैसला लग सकता है, पर जो बिहार में भाजपा की राजनीति को देख रहे हैं, उनके लिए यह सामान्य-सी बात है। भाजपा पिछड़ी व अत्यन्त पिछड़ी जातियों के बीच पिछले दो दशक से अपना जनाधार बढ़ाने में एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। राज्य में वह अपने उस इतिहास से खुद को दूर करना चाह रही है, जिसमें उसे केवल तथाकथित उच्च जाति सवर्णों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था। इसमें एक हद तक उसे कामयाबी भी मिली है, पर अभी भी पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के वोट अधिकांशतः राजद व वाम दलों के बीच बँट जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों का वोट बैंक साधने के लिए ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला लिया गया है। कर्पूरी ठाकुर उत्तर भारत में विशेषकर बिहार व झारखण्ड में पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर अब भी याद किये जाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाये तो भाजपा व संघ ने पहले राम मन्दिर उद्घाटन के जरिये कमण्डल की राजनीति को साधा और अब, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मण्डल की राजनीति में भी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है।
’भारतीय बुर्जुआ राजनीति में दो शब्दों, मण्डल और कमण्डल को अक्सर एक दूसरे के विलोम के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन वास्तव में दोनों ही राजनीतिक धाराओं का यह अन्तर केवल सतही है और वस्तुतः ये एक दूसरे के पूरक का काम करती हैं। पिछले 40 वर्षों के राजनीतिक इतिहास ने तो यही दर्शाया है कि दोनों ही धाराएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज भारत में कमण्डल की राजनीति के जरिये फासीवाद की विषबेल भी मण्डल की राजनीति के कारण बनी जमीन पर ही पनपी है। कभी मण्डल की राजनीति के जरिये कमण्डल का जवाब देने की बात करने वाले नीतीश कुमार व शरद यादव भी सत्ता का सुख पाने के लिए भाजपा के साथ गलबहियाँ करने से नहीं हिचके। और यह अनायास नहीं था, बल्कि वर्गीय राजनीति में इसकी वजहें निहित थीं।’
वैसे इस प्रकरण ने नीतीश कुमार को भी अपने पलटने को सही ठहराने का एक बहाना दे दिया, कर्पूरी ठाकुर के बहाने अपनी सभाओं में नीतीश कुमार एक तरफ तो प्रधानमन्त्री मोदी के तारीफों के पुल बाँधते गए और दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव पर दबे सुर में कटाक्ष करते रहे।
जातीय जनगणना के उपरान्त भाजपा के भी कान खड़े हो गए थे। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में सिर्फ अत्यन्त पिछड़ी जातियाँ कुल जनसंख्या के 36 प्रतिशत के करीब है। अगर अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को भी शामिल कर लिया जाये, तो यह आँकड़ा 61 फीसदी तक पहुँच जाता है। इस जातीय जनगणना के बाद, देश भर में इसे करने को लेकर भी बात उठने लगी थी। सूबे में भी इस जनगणना के तत्काल बाद सरकारी नौकरियों में पिछड़ी, अत्यन्त पिछड़ी, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण को 65 प्रतिशत तक करने के लिए बकायदा विधानसभा में बिल भी पास कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा करने से सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजद भी थोड़ी असहज हुयी, क्योंकि यह उसके परम्परागत वोटबैंक में सेंधमारी का प्रयास था।
वैसे यह भी पहली बार हुआ जब किसी को भारत रत्न देने के उपरान्त प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा लिखा गया कोई लेख अखबारों में छापा गया हो। इस लेख में कर्पूरी ठाकुर के सादे जीवन व उनके व्यक्तित्व का बखान है पर उनकी राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा के बिहार का नेतृत्व ने भी कर्पूरी ठाकुर के ऊपर राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित किये। उनको “अपना नेता” साबित करने की हर सम्भव कोशिश की। जनता को यह सन्देश देने का प्रयास किया गया कि भाजपा व संघ पिछड़ी व अत्यन्त पिछड़ी जातियों के साथ खड़ी है। लेकिन अगर इनके इतिहास को पलट देखा जाये तो फिर इनकी सच्चाई सामने आती है।
इसके पहले कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को भी समझना जरूरी है। कर्पूरी ठाकुर जेपी व लोहिया ब्राण्ड नामधारी समाजवादी धारा के ही नेता थे। कर्पूरी ठाकुर अपने समकालीन नामधारी समाजवादी नेताओं से अलग इस मायने में थे कि उन्होंने बिहार में अपनी राजनीति के साथ कांशीराम सरीखी अस्मितावादी राजनीति का घाल-मट्ठा बनाया। नक्सलबाड़ी आन्दोलन के समय वंचित तबकों की एक ऐसी आबादी थी जो अपने हक और अधिकारों को लेकर जागृत हुई थी और इस आन्दोलन में शामिल भी हुई थी। लेकिन क्रान्तिकारी वाम के क्रान्ति की मंजिल, भारतीय समाज के चरित्र की पहचान के सवाल पर पुराने पड़ चुके कठमुल्लावादी चैखटे में कैद रहने और साथ ही दुस्साहसवादी विचलन के कारण यह आन्दोलन अपनी व्यापकता के बावजूद आगे नहीं जा सका। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की असफलता से खाली स्थान का फायदा बिहार में जाति आधारित अस्मितावादी राजनीति को मिला, कर्पूरी ठाकुर का आधार भी इसी आबादी के बीच से पनपा।
आपातकाल के पहले और बाद में भी आर.एस.एस. के चुनावी फ्रण्ट जनसंघ के समर्थन वाली साझा राज्य सरकारों में कर्पूरी ठाकुर मन्त्री रहे। गाँधी की हत्या के बाद तत्कालीन जनसंघ के जरिये संघ परिवार को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने का एक श्रेय काफी हद तक इन नामधारी समाजवादियों को जाता है। पहले राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर सरीखे नेता जनसंघ के सम्पर्क में बने रहे। हाँ, यह जरूर है कि आगे चलकर जनसंघ के साथ कर्पूरी ठाकुर के सम्बन्ध इस हद तल्ख हुए कि संघ के नेताओं ने उनपर निजी हमले किये और उन्हें सीधे-सीधे गालियाँ दी लेकिन ऐसा तो कई समाजवादी नेताओं के साथ हुआ और इससे उनके इस ऐतिहासिक अपराध में कोई कमी नहीं आती है।
बहरहाल, बिहार में 1967 में महामाया प्रसाद सरकार में कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षामन्त्री रहते हुए जब उर्दू को सूबे की दूसरी राजभाषा बनाने का फैसला लिया, तब संघ के नेताओं ने उनका विरोध किया और उन्हें “मौलाना कर्पूरी ठाकुर” कहकर सम्बोधित किया। 1977 में बिहार में बनी जनता पार्टी की सरकार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमन्त्री थे। उनके ही कार्यकाल में 1978 में पिछड़ी व अत्यन्त पिछड़ी जातियों की स्थिति पर मुँगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आयी। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पिछड़ी और अत्यन्त पिछड़ी जातियों को अलग-अलग आरक्षण देने की बात कर्पूरी ठाकुर ने की। इसी फैसले को बाद में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला कहा गया। 1979 में जब पिछड़ों और अत्यन्त पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात उठाई गयी, तो सबसे पहले जनसंघ और भविष्य के भाजपाइयों ने ही विरोध के स्वर उठाये थे और आज पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के वोट को लपकने के लिए वे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं। इस फॉर्मूले के विरोध में तत्कालीन जनसंघ के नेता कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर की सरकार से समर्थन खींच लिया गया, जिससे कर्पूरी ठाकुर की सरकार अल्पमत में आ गयी और गिर गयी। बात यही तक नहीं रुकी, राज्य भर में इस फॉर्मूले के विरोध में संघ के नेताओं की शह पर हिंसक प्रदर्शन हुए। उस वक्त संघ के नेता “ये आरक्षण कहाँ से आयी, कर्पूरी ठाकुर के माई बियायी” जैसे स्त्री विरोधी नारों से कर्पूरी ठाकुर का विरोध करते थे। इस दौरान बिहार की पिछड़ी और अत्यन्त पिछड़ी आबादी के समक्ष संघ की जो सवर्णवादी और आरक्षण-विरोधी छवि बनी, वह आज भी एक हद तक बरकरार है। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण पर बिल लाने के बाद पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात आगे चलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। यहाँ तक की तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई (जो उस वक्त तक आरक्षण के पक्ष में नहीं थे) के निर्देश पर बी.पी मण्डल की अध्यक्षता में “सोशली एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन” का गठन किया गया, जिसे मण्डल कमीशन भी कहा जाता है। परन्तु, 1980 में इस कमीशन की रिपोर्ट आने और इसके सिफारिशों को लागू करने के पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिर गयी। फिर अगले एक दशक तक इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए पहले इन्दिरा गाँधी की सरकार और बाद में राजीव गाँधी की सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा।
यही वह समय था, जब मण्डल आयोग के बहाने बिहार में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अपना कद देश की राजनीति में बढ़ा रहे थे। भाजपा तात्कालिक तौर पर मण्डल की राजनीति के खिलाफ राम मन्दिर के बहाने कमण्डल की राजनीति को हवा दे रही थी। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की घोषणा की, तब भाजपा ने इसका मुकाबला राम मन्दिर आन्दोलन मे तेजी लाते हुए देश भर में रथयात्रा निकाल कर किया। इस यात्रा के दौरान उस वक्त भाजपा व संघ के नेता अपने भाषणों में मण्डल आयोग की सिफारिशों को हिन्दू विरोधी करार देते थे। कर्पूरी ठाकुर को इसका जिम्मेदार बताते थे। स्पष्ट है कि आज पिछड़ों के वोट बैंक में अपनी सेंध को बढ़ाने के लिए भाजपा को अपने सुर बिल्कुल बदलने की जरूरत पड़ी है, तो उसने बदल दिये हैं। इतिहास ने दिखलाया कि मण्डल की राजनीति ने भी अन्ततरू फासीवादी शक्तियों के लिए एक वोट बैंक तैयार करने का काम किया। तात्कालिक तौर पर पूँजीवादी राजनीति के दायरे के भीतर भी मण्डल व कमण्डल का अन्तरविरोध केवल आर्थिक संकट से ग्रस्त देश में जनता के असन्तोष को अस्मितावादी पूँजीवादी राजनीति के दायरे में सोख लेने के लिए ही था। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने इस मसले पर अपने सुर बदले हैं, वह उसकी धुर अवसरवादी फासीवादी राजनीति की सच्चाई को बेपर्द करता है।
भाजपा व संघ ऐसे राजनीतिक स्टण्ट करके खुद को पिछड़ी व दलित जातियों का हितैषी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि वर्ष 2014 के बाद से, यानी मोदी के सत्तासीन होने के बाद से, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अपराधों में आज क्रमशः 27.3 और 20.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अकेले वर्ष 2021 में 50,900 दलित विरोधी अपराध दर्ज किये गए। आज भी ऊना काण्ड लोगों की स्मृतियों में भयावाह सत्य की तरह जिन्दा है। एक तरफ तो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं तो दूसरी ओर आर्थिक तौर पर भी उनके हालात बदतर होते गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 6 में से 5 गरीब व्यक्ति (मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इण्डेक्स के हिसाब से) तथाकथित निम्न व अनुसूचित जातियों व जनजातियों से आते है। सरकारी नौकरियों में भी पिछले दस सालों में पिछड़ी जातियों की भागीदारी का स्तर और नीचे गया है। भारत सरकार के आँकड़ों के ही अनुसार, 2014 में सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से की गई कुल सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 17.97 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों की नुमाइन्दगी 8.26 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों की नुमाइन्दगी 31.50 प्रतिश्ज्ञत थी। लेकिन 2021 में प्रतिनिधित्व का यह प्रतिशत घटकर अनुसूचित जातियों के लिए 17.07 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.57 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30.68 प्रतिशत हो गया है।
हम जानते हैं कि भारत में पूँजीवाद ने हमेशा ही सवर्णवाद और उच्च जाति के श्रेष्ठताबोध का अपने लिए इस्तेमाल किया है और उसे प्रतिसन्तुलित करने के लिए दलितों, आदिवासियों, औरतों, व गरीब वर्गों से आने वाले पिछड़ी जातियों की आबादी को अस्मितावाद और प्रतीकवाद की अन्धी गलियों में घुमाया है। भाजपाई फासीवादी तो इस काम को करने की कुशलता को नयी ऊँचाइयों पर ले गये हैं। ऊपर बताये आँकड़ों से भाजपाई फासीवाद का गन्दा दलित-विरोधी, आदिवासी-विरोधी चेहरा दिख जाता है। अपनी इस सवर्णवादी सच्चाई को छिपाने के लिए आज दलित व पिछड़ी जातियों के बीच भाजपा व संघ अस्मितावाद और प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। भारत की चुनावी राजनीति इस बात का पुख़्ता प्रमाण है कि अस्मितावादी राजनीति देर-सबेर हमेशा ही दक्षिणपन्थी राजनीति में समाहित हो जाती है। इसलिये अगर कोई यह सोच रहा है कि जेपी-लोहिया ब्राण्ड नामधारी समाजवादियों की मण्डल की राजनीति से भाजपा व संघ की फासीवादी राजनीति का मुकाबला किया जा सकता है, तो फिर वह ख़ुद को धोखे में रख रहा है। इसके अतिरिक्त मण्डल की राजनीति की वापसी जैसी कोई चीज अगर हो भी तो शायद इसे 90 के दशक जैसा जन समर्थन नहीं मिल पायेगा। उस दौर में दलित छात्र और युवाओं ने मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आन्दोलनों में शिरकत की, क्योंकि तब रोजगार मिलने की खोखली ही सही, पर आशा थी। आज तीन दशक के बाद हालात बिल्कुल अलग हैं। आज देश में रोजगार को स्थिति से हम सभी वाकफि हैं। सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र रोजगार के अवसर लगातार घटे है। ऐसे में आरक्षण की बात ही बेमानी हो जाती है। आरक्षण की सीमा बढाकर अगर 70 फीसदी भी कर दी जाये तो भी पिछड़ी जातियों व दलितों के 10 प्रतिशत युवाओं को नौकरी नहीं दी जा सकती है। साथ ही, पिछले 30 वर्षों में विशेषकर पिछड़ी जातियों के बीच से एक धनी फार्मर-कुलक वर्ग भी पैदा हुआ है, जिसे प्रतिक्रियावादी राजनीति ने अपने दायरे में समेटा है। उसका एक हिस्सा शहरी नौकरियों में भी गया है और व्यवसाय में भी गया है। समाज में मण्डल की राजनीति का वर्गीय आधार भी पहले के मुकाबले कमजोर पड़ा है।
आज इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई व्यापक मेहनतकश जनता के आर्थिक व राजनीतिक हितों की लड़ाई में शामिल हुए बिना नहीं लड़ी जा सकती है। भाजपा की साम्प्रदायिक फासीवादी राजनीति का जवाब सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी राजनीति द्वारा ही दिया जा सकता है। और कोई भी दूसरा रास्ता इस फासीवादी विषबेल को खाद पानी देने का ही काम करेगा। दलितों व आदिवासियों को, स्त्रियों को व आम मेहनतकश घर से आने वाली पिछड़ी जातियों के लोगों को सामाजिक दमन और आर्थिक शोषण दोनों से ही मुक्ति पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी इस स्थिति को बनाये रखने में मौजूदा शासक वर्ग, यानी पूँजीपति वर्ग का हित है। यह बात दीगर है कि अपनी व्यवस्था द्वारा ही पैदा किये गये इस सामाजिक दमन और आर्थिक शोषण पर हमारे असन्तोष को गलत दिशा में मोड़ देने के लिए किसी न किसी किस्म की अस्मितावादी राजनीति को हमारे बीच फैलाया जाता है, चाहे वह मण्डल की राजनीति हो या कमण्डल की।
(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इससे हमारे प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं है।)